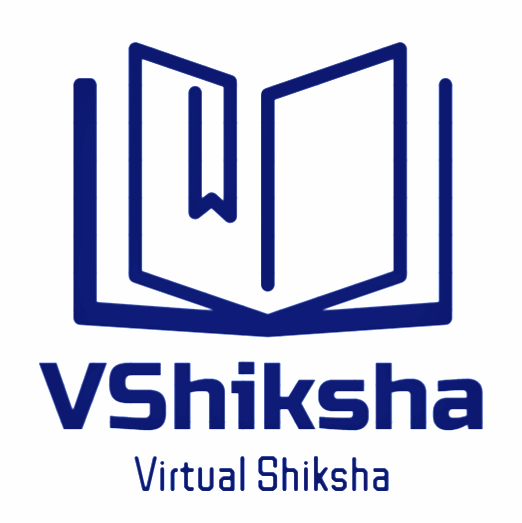सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी के भेदभाव-विरोधी नियमों को हरी झंडी दी
परिचय
नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2025 — एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और जाति, लिंग, विकलांगता और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव से निपटने के लिए बनाए गए अपने 2025 मसौदा विनियमों को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया है। इस कदम को देश भर के छात्रों के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि विनियमों के दायरे और कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।
24 अप्रैल, 2025 को दिया गया यह फैसला 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तड़वी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब है। दोनों छात्रों की 2016 में आत्महत्या कर ली गई थी, उनके परिवारों ने आरोप लगाया था कि जाति-आधारित भेदभाव ने उनकी दुखद मौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फैसला उच्च शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, साथ ही भेदभाव से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में चल रही बहस को भी उजागर करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
जनहित याचिका हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी की मां अबेदा सलीम तड़वी ने शुरू की थी। दोनों छात्रों को कथित तौर पर उनकी जातिगत पहचान के कारण गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उनके परिवारों का दावा है कि 2016 में उनकी आत्महत्या का कारण यही था। 2019 में दायर मुकदमे में मौजूदा नियमों, विशेष रूप से यूजीसी के 2012 के "समानता को बढ़ावा देने के नियम" की ऐसी त्रासदियों को रोकने में विफलता की आलोचना की गई। इसने हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपायों की मांग की।
जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी और बढ़ गई, जब उसने यूजीसी को छह सप्ताह के भीतर मजबूत भेदभाव-विरोधी विनियमों का मसौदा तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिसमें कार्रवाई योग्य समाधानों पर जोर दिया गया। 24 अप्रैल, 2025 का फैसला इस निर्देश पर आधारित है, जो यूजीसी को अपने 2025 के मसौदा विनियमों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विवरण
24 अप्रैल, 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यूजीसी को “यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2025” को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने की अनुमति दी। यह निर्णय एक सुनवाई के दौरान आया, जिसमें यूजीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अधिसूचना प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।
न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और अधिवक्ता प्रसन्ना एस. तथा दिशा वाडेकर द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने तक अधिसूचना को स्थगित करने की मांग की गई थी। 24 मार्च, 2025 को गठित एनटीएफ को शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और भेदभाव को दूर करने का काम सौंपा गया है। न्यायालय ने कमजोर छात्रों की सुरक्षा के लिए विनियमों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "जब तक कार्य बल अपनी सिफारिशें नहीं देता, तब तक विनियम बेजुबानों की मदद करेंगे"।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये विनियम भविष्य में एनटीएफ की किसी भी सिफारिश के पूरक होंगे और हितधारकों को अधिसूचना के बाद संशोधनों का सुझाव देने या एनटीएफ को इनपुट प्रदान करने की अनुमति दी। इस लचीलेपन का उद्देश्य तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए चिंताओं को दूर करना है।
2025 मसौदा विनियमों की मुख्य विशेषताएं
प्रोफ़ेसर शैलेश एन. ज़ाला की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए “यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2025” में उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। यह मसौदा 27 फ़रवरी, 2025 को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा | अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरुद्ध भेदभाव तक सीमित, 2012 के विनियमों की तुलना में इसका दायरा सीमित है। |
| सामान्य भेदभाव | इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य कारकों के आधार पर अनुचित व्यवहार शामिल है, जो सभी हितधारकों (छात्र, संकाय, कर्मचारी) पर लागू होता है। |
| इक्विटी समितियां | समान अवसर केन्द्रों के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, जिसमें दो नागरिक समाज प्रतिनिधि, दो छात्र प्रतिनिधि, चार संकाय सदस्य और संस्था प्रमुख पदेन प्रमुख होंगे। |
| झूठी शिकायतों के लिए दंड | इसमें जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव है, हालांकि "झूठी शिकायत" की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव है, जिससे संभावित दुरुपयोग की चिंता बढ़ रही है। |
| यूजीसी शक्तियां | यह यूजीसी को गैर-अनुपालन विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने का अधिकार देता है, तथा प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाता है। |
2012 के नियमों की तुलना में, जिसमें भेदभाव को व्यापक रूप से “किसी भी भेद, बहिष्कार, सीमा या वरीयता” के रूप में परिभाषित किया गया था, जो समानता को बाधित करता है, 2025 का मसौदा “किसी भी हितधारक” के दायरे को बढ़ाता है, लेकिन जाति-आधारित भेदभाव को एससी/एसटी तक सीमित कर देता है। इस बदलाव ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या यह जातिगत पूर्वाग्रह के सभी रूपों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है।
चिंताएं और आलोचनाएं
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के दौरान मसौदा विनियमों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ व्यक्त कीं। उन्होंने तर्क दिया कि रैगिंग, यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और अन्य पूर्वाग्रहों के लिए विनियमों को एक ही ढांचे में मिलाने से प्रशासनिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भेदभाव के प्रत्येक रूप को उसकी अनूठी प्रकृति के कारण अलग-अलग तरीके से संभालने की आवश्यकता होती है। जयसिंह ने 2012 के विनियमों से जातिगत भेदभाव के विशिष्ट उदाहरणों को हटाने की भी आलोचना की, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण से इनकार करना, जो प्रवर्तन के लिए स्पष्टता प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त, जाति-आधारित भेदभाव की संकीर्ण परिभाषा की भी जांच की गई है। 2012 के विनियमों में जाति, पंथ, भाषा, धर्म, जातीयता, लिंग और विकलांगता सहित कई व्यापक आधार शामिल थे, और छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आलोचकों का तर्क है कि जाति-आधारित भेदभाव को एससी/एसटी तक सीमित करने से समान पूर्वाग्रहों का सामना करने वाले अन्य हाशिए के समूह बाहर हो सकते हैं।
झूठी शिकायतों पर दंड लगाने के प्रावधान ने संभावित दुरुपयोग के बारे में भी चिंताएँ पैदा की हैं, क्योंकि मसौदे में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि झूठी शिकायत क्या होती है। यह अस्पष्टता वास्तविक शिकायतों को रोक सकती है, खासकर हाशिए पर पड़े छात्रों से।
राष्ट्रीय कार्य बल और व्यापक संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उच्च शिक्षा में भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। 24 मार्च, 2025 को न्यायालय ने चार महीने के भीतर व्यापक उपायों का प्रस्ताव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक एनटीएफ का गठन किया। एनटीएफ में उच्च शिक्षा, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा कानूनी मामलों के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका गठन एससी/एसटी समुदायों के दो आईआईटी दिल्ली छात्रों की 2023 में आत्महत्या की पुलिस जांच के बाद हुआ, जिसमें चल रहे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
न्यायालय के इस निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि यूजीसी के नियम एनटीएफ की सिफारिशों के साथ-साथ काम करेंगे, जिससे कैंपस में समानता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार होगा। ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ भी संरेखित हैं, जो शिक्षा में समावेशिता और समानता पर जोर देती है।
उच्च शिक्षा पर प्रभाव
2025 के विनियमनों की अधिसूचना से उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न से निपटने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रैगिंग, यौन उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने और संबोधित करने के लिए इक्विटी समितियों जैसे मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। गैर-अनुपालन संस्थानों की मान्यता रद्द करने का यूजीसी का अधिकार जवाबदेही की एक परत जोड़ता है, जो संभावित रूप से संस्थानों को अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करता है।
हालांकि, इन विनियमों की प्रभावशीलता उनके कार्यान्वयन और हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के समाधान पर निर्भर करेगी। शैक्षणिक समुदाय, छात्र निकाय और नागरिक समाज इस प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये उपाय अधिक समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देंगे। अधिसूचना के बाद संशोधनों का सुझाव देने के लिए हितधारकों के लिए अवसर भेदभाव के विविध रूपों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए विनियमों को परिष्कृत करने का मार्ग प्रदान करता है।
निष्कर्ष
यूजीसी को अपने 2025 के भेदभाव-विरोधी विनियमों को अधिसूचित करने की अनुमति देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय उच्च शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद मौतों से प्रेरित, यह निर्णय कमजोर छात्रों की सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि विनियम महत्वपूर्ण उपाय पेश करते हैं, उनके दायरे और प्रशासनिक व्यवहार्यता के बारे में चिंताएँ निरंतर संवाद और परिशोधन की आवश्यकता को उजागर करती हैं। जैसा कि यूजीसी विनियमों को अधिसूचित करने की तैयारी कर रहा है, अब ध्यान पूरे भारत में सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत परिसर बनाने के लिए उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।